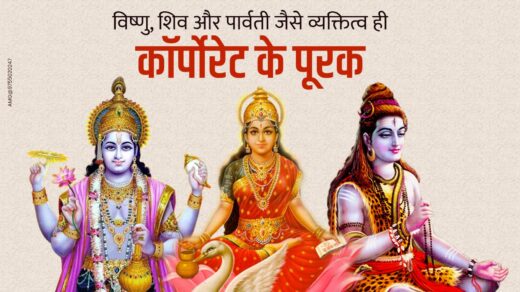भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक परिदृश्य में घुमंतु समाज का स्थान अद्वितीय और गहरा है। यह कोई अलग या पृथक वर्ग नहीं, बल्कि भारत की सभ्यता की जीवंत धारा है — एक ऐसी धारा जो हजारों वर्षों से घूमती रही है, लेकिन कभी भी अपनी जड़ों से विचलित नहीं हुई। नट, सपेरा, बंजारा, लोहार, बैरवा, बावरिया, गारसिया, जोगी, टोड़ा, कट्टन, रावत, बेल्ला और असंख्य अन्य समुदाय — ये वे लोग हैं जिन्होंने भारत की सड़कों को अपना घर बनाया, गाँवों को अपना मंच, जंगलों को अपना आश्रय और तीर्थस्थलों को अपना आध्यात्मिक आधार माना। पीढ़ी दर पीढ़ी वे अपनी कला, संस्कृति, ज्ञान और जीवनशैली को बिना किसी स्थायी संरचना के बीच-बीच में जीवित रखा है।
उनके गीत भारत की मिट्टी की गहराई से निकले हैं, उनके नृत्य प्रकृति के ताल पर थिरकते हैं, उनके हस्तशिल्प सदियों के अनुभव का सार हैं, और उनकी जीवनशैली एक ऐसा जीवंत इतिहास है जो किताबों में नहीं, बल्कि उनके प्रत्येक कदम में छिपा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जिस भारत ने इन्हें अपनी संस्कृति का हिस्सा माना, वही आधुनिक भारत आज इन्हें अपनी मुख्यधारा से दूर रख रहा है।

ये समुदाय केवल आर्थिक रूप से पिछड़े नहीं हैं — वे ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित, सामाजिक भेदभाव का शिकार और मानवाधिकारों से वंचित रहे हैं। उनकी गतिशील जीवनशैली, जो कभी उनकी ताकत थी, आज उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पहचान, आवास और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएँ उनके लिए अभी भी सपने बनी हुई हैं। उनके पास न तो आधार कार्ड है, न बैंक खाता, न बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र — और फिर भी वे भारत के नागरिक हैं।
उनकी पारंपरिक कला, लोकगीत, नृत्य, हस्तशिल्प, पशुपालन और प्राकृतिक ज्ञान प्रणाली भारत की सांस्कृतिक आत्मा का अहम हिस्सा हैं। ये कलाएँ केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक सम्पूर्ण जीवन दर्शन का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन आज के शहरीकृत, डिजिटल और व्यवस्थित भारत में इनकी जगह नहीं है। उनके साथ हो रहा विस्थापन, उपेक्षा और सामाजिक भेदभाव कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक नीतिगत उपेक्षा का परिणाम है।
इस लेख में, हम घुमंतु समाज के इतिहास को मानव इतिहास के आरंभ से लेकर आज के डिजिटल युग तक गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि मानवता के प्रारंभ में घुमंतु जीवनशैली कैसे उभरी, कैसे भारत के प्राचीन ग्रंथों — वेदों, रामायण, महाभारत — में इनके जीवन के चित्रण मिलते हैं, कैसे मुगल और ब्रिटिश काल में इनकी भूमिका बदली, और कैसे आजाद भारत में भी इन्हें न्याय नहीं मिला।
साथ ही, हम यह भी विस्तार से जानेंगे कि भारत सरकार ने इन समुदायों के उत्थान के लिए कौन-कौन से कदम उठाए हैं — गोविंदा नायक आयोग से लेकर NTDFA, आधार कार्ड, आयुष्मान भारत तक — और इनकी प्रभावशीलता क्या रही। आखिर, आज के इंटरनेट युग में, जहाँ हर चीज डिजिटल हो रही है, घुमंतु समाज की स्थिति क्या है? क्या वे इस डिजिटल विभाजन (Digital Divide) से पार पा रहे हैं? क्या उनकी पहचान, शिक्षा और आजीविका में सुधार हो रहा है?
यह लेख केवल एक जानकारी का संकलन नहीं है — यह एक आह्वान है। एक आह्वान उस भारत के प्रति, जो न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध हो, बल्कि सांस्कृतिक रूप से समावेशी भी हो। एक आह्वान उस समाज के प्रति, जो अपने हर नागरिक को गरिमा से जीने का अधिकार दे। क्योंकि जब तक घुमंतु समाज को उसकी पहचान, गरिमा और अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक भारत का विकास अधूरा रहेगा।

मानव इतिहास का आरंभ: घुमंतु जीवनशैली की उत्पत्ति — मानवता का प्रथम आधार
घुमंतु जीवनशैली कोई आधुनिक घटना नहीं है, न ही यह केवल भारत की सामाजिक विशेषता है। यह तो मानव इतिहास के साथ-साथ उत्पन्न हुई — यह मानवता की प्रथम और सबसे प्राकृतिक जीवनशैली है। लगभग 2 लाख वर्ष पहले, जब मानव प्रजाति होमो सेपियंस (Homo Sapiens) अफ्रीका की घाटियों में उत्पन्न हुई, तो उसकी जीवनशैली पूर्णतः घुमंतु थी। यह न केवल एक आर्थिक आवश्यकता थी, बल्कि प्रकृति के साथ एक गहरे सामंजस्य का प्रतीक थी।
उस समय मानव अभी स्थायी बस्तियाँ बसाने, खेती करने या पशुपालन के चरण में नहीं पहुँचा था। उसकी अस्तित्व की सारी आशाएँ थीं — भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने में। यह यात्रा कोई यादगार पल के लिए नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच का संतुलन बनाए रखने के लिए थी। इस प्रकार के समुदायों को इतिहासकार “शिकारी-संग्राहक समुदाय” (Hunter-Gatherers) कहते हैं — एक ऐसा जीवन जो प्रकृति के ताल पर चलता था, उसके संसाधनों का सम्मान करता था और अत्यधिक उपभोग से बचता था।

ये समुदाय जंगलों में फल, जड़ी-बूटियाँ, शहद, अंडे और छोटे जानवरों का शिकार करके अपनी आजीविका चलाते थे। वे प्रकृति के ऋतु-चक्र को जानते थे — कब फल लगेंगे, कब पक्षी आएंगे, कब नदियाँ भर जाएंगी। उनका ज्ञान पुस्तकों में नहीं, बल्कि अनुभव और मौखिक परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होता था। वे न तो भूमि के मालिक थे, न ही उन्होंने कभी प्रकृति पर अधिकार जताया। वे उसके सहयात्री थे
उनका आवास भी इसी गतिशीलता के अनुरूप था। वे कोई स्थायी घर नहीं बनाते थे। उनका घर था — गुफाएँ, पेड़ों के नीचे का स्थान, झोपड़ियाँ, छप्पर या प्राकृतिक आश्रय। वे जब तक किसी स्थान पर संसाधन उपलब्ध रहते, वहाँ ठहरते थे। जैसे ही संसाधन कम होने लगते, वे आगे बढ़ जाते थे। यह गतिशीलता उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। यह उन्हें जलवायु परिवर्तन, आपदाओं और प्राकृतिक बदलावों के प्रति अत्यधिक अनुकूलनशील बनाती थी।
लेकिन यह घुमंतु जीवन केवल भौतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं था। इसके साथ-साथ एक समृद्ध सांस्कृतिक जीवन भी विकसित हुआ। उनकी संस्कृति, कला और धर्म उनके यात्रा मार्गों के साथ-साथ विकसित होते रहे। गुफाओं की दीवारों पर चित्र, नृत्य जो ऋतुओं के आगमन का उत्सव मनाते थे, गीत जो शिकार की कहानियाँ सुनाते थे, और आध्यात्मिक अनुष्ठान जो प्रकृति के देवताओं को समर्पित होते थे — ये सब उस घुमंतु जीवन का हिस्सा थे।

आज के घुमंतु समाज के साथ इस प्राचीन जीवनशैली की समानता आश्चर्यजनक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक निरंतरता का प्रमाण है। आज भी, बंजारा, बैरवा, बावरिया, गारसिया और अन्य घुमंतु समुदाय उसी धरोहर के वाहक हैं। वे भी घूमते हैं, प्रकृति पर निर्भर हैं, मौसम के अनुसार अपने मार्ग तय करते हैं, और अपनी संस्कृति को गीत, नृत्य और कथाओं के माध्यम से जीवित रखते हैं। उनके गीत भी उसी तरह प्रकृति की स्तुति करते हैं, उनके नृत्य भी उसी तरह ऋतुओं का उत्सव मनाते हैं, और उनकी आजीविका भी प्रकृति के साथ सामंजस्य में चलती है।
इस प्रकार, घुमंतु जीवनशैली मानव इतिहास की नींव है। यह न केवल एक जीवन तरीका है, बल्कि मानवता के उद्भव का एक जीवंत प्रमाण है। जब हम आज बंजारा के गीत सुनते हैं या बैरवा के नृत्य को देखते हैं, तो हम वास्तव में 2 लाख साल पुराने मानव अनुभव की आवाज सुन रहे होते हैं। यह जीवनशैली नष्ट नहीं हुई, बस आधुनिक सभ्यता के तेजी से बदलते ढांचे में उसे अनदेखा कर दिया गया। लेकिन वह अभी भी जीवित है — भारत की सड़कों पर, जंगलों के किनारे, गाँवों के बाहरी इलाकों में — एक ऐसी धारा जो मानवता के प्रारंभ से लेकर आज तक बहती आई है।
प्राचीन भारत: वैदिक काल से महाकाव्यों तक — घुमंतु जीवनशैली का ऐतिहासिक आधार
भारत के सांस्कृतिक इतिहास में घुमंतु जीवनशैली की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उनका उल्लेख सबसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। वैदिक काल से लेकर महाकाव्यों तक, घुमंतु जीवन को न केवल स्वीकार किया गया, बल्कि उसे एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी प्राप्त था। यह जीवनशैली केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं थी, बल्कि एक जीवन दर्शन, एक सामाजिक भूमिका और एक सांस्कृतिक वाहक के रूप में विकसित हुई।

वैदिक काल: घुमंतु जनजातियों का प्राचीन उल्लेख
वैदिक ग्रंथों में घुमंतु समुदायों के लिए विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में “मृगवाले”, “वाणिक”, “गवयन”, “मेधवी”, “राब्धि” और “किकट” जैसे नामों का उल्लेख मिलता है। ये नाम ऐसे समुदायों को दर्शाते हैं जो घूमते रहते थे, प्रकृति पर निर्भर थे और अपनी आजीविका के लिए विभिन्न गतिविधियों पर निर्भर थे।
- मृगवाले — जंगली जानवरों का शिकार करने वाले घुमंतु शिकारी।
- वाणिक — घूमते हुए व्यापारी या वाणिज्य करने वाले समूह।
- गवयन — गायों के पालन और उनके साथ घूमने वाले पशुपालक।
- मेधवी — ज्ञानी, लेकिन घुमंतु स्वभाव वाले ऋषि या विद्वान।
इन समुदायों को वैदिक समाज में कभी भी पूर्णतः बाहर नहीं रखा गया था। वे समाज के बाहरी किनारे पर रहते थे, लेकिन उनके साथ आदान-प्रदान होता था — वे वनस्पतियाँ, शहद, चमड़ा, औषधियाँ और मनोरंजन के लिए कला प्रदान करते थे, और समाज उन्हें अनाज, कपड़े और सुरक्षा देता था। यह एक पारस्परिक संबंध था, जो घुमंतु जीवन को समाज का एक अभिन्न हिस्सा बनाता था।
प्राचीन भारत: वैदिक काल से महाकाव्यों तक — घुमंतु जीवनशैली का ऐतिहासिक आधार
भारत के सांस्कृतिक इतिहास में घुमंतु जीवनशैली की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उनका उल्लेख सबसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। वैदिक काल से लेकर महाकाव्यों तक, घुमंतु जीवन को न केवल स्वीकार किया गया, बल्कि उसे एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी प्राप्त था। यह जीवनशैली केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं थी, बल्कि एक जीवन दर्शन, एक सामाजिक भूमिका और एक सांस्कृतिक वाहक के रूप में विकसित हुई।
महाभारत और रामायण: घुमंतु जीवनशैली के शास्त्रीय उदाहरण
(क) रामायण: भगवान राम और वानर सेना — घुमंतु जीवन का आदर्श चित्रण

रामायण में घुमंतु जीवनशैली का सबसे प्रभावशाली चित्रण भगवान राम के वनवास और वानर सेना के साथ उनके सहयोग में देखने को मिलता है। जब राम, सीता और लक्ष्मण ने 14 वर्ष का वनवास शुरू किया, तो वे भी एक प्रकार की घुमंतु जीवनशैली अपना लेते हैं। वे एक स्थान पर नहीं ठहरते, बल्कि जंगलों, नदियों और पहाड़ों के बीच यात्रा करते हैं। उनका आवास गुफाएँ, आश्रम और प्राकृतिक आश्रय होते हैं। उनकी आजीविका फल-फूल, जड़ी-बूटियों और भिक्षा पर आधारित होती है।
यह वनवास न केवल एक दंड नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन है जो प्रकृति के साथ एकता, त्याग और आध्यात्मिक गहराई को दर्शाता है — जो घुमंतु जीवन के मूल सिद्धांतों से मेल खाता है।
इसी दौरान, वानर समुदाय — सुग्रीव, हनुमान, नल, नील, अंगद आदि — एक ऐसे समाज के प्रतीक हैं जो पहाड़ों, जंगलों और नदियों के बीच जीते थे।
- उनका आवास स्थायी नहीं था। वे प्राकृतिक गुफाओं, पेड़ों के नीचे और पहाड़ी टीलों पर रहते थे।
- उनकी आजीविका प्रकृति पर आधारित थी — फल, फूल, शहद, जड़ी-बूटियाँ और छोटे जानवरों का शिकार।
- वे संगीत, नृत्य, शिल्प और युद्धकला में अत्यंत निपुण थे।
- उनका समाज लचीला था — वे जब चाहते घूमते थे, लेकिन अपनी संस्कृति और पहचान को बनाए रखते थे।
वानर सेना के जीवन में घुमंतु जीवनशैली के सभी तत्व मौजूद हैं: गतिशीलता, प्रकृति पर निर्भरता, सामूहिक जीवन, सांस्कृतिक समृद्धि और सामाजिक गतिशीलता। आज के बंजारा, बैरवा और बावरिया समुदाय भी इसी प्रकार के जीवन को जीते हैं — वे घूमते हैं, प्रकृति पर निर्भर हैं, और अपनी संस्कृति को गीत-नृत्य से जीवित रखते हैं।
(ख) महाभारत: पांडवों का वनवास — घुमंतु जीवन का आध्यात्मिक रूप

महाभारत में पांडवों का 12 वर्ष का वनवास घुमंतु जीवनशैली का एक आध्यात्मिक और दार्शनिक उदाहरण है। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ने अपने वनवास के दौरान भारत के विभिन्न जंगलों, नदियों, पहाड़ों और तीर्थस्थलों की यात्रा की। वे किसी एक स्थान पर नहीं ठहरे, बल्कि लगातार घूमते रहे।
- उनका आवास था — गुफाएँ, ऋषि-मुनियों के आश्रम, पेड़ों के नीचे के आश्रय।
- उनकी आजीविका थी — भिक्षा, शिकार, फल-फूल और ऋषियों के साथ साझा भोजन।
- उन्होंने अपनी कला और कौशल बनाए रखे — अर्जुन ने इंद्रलोक जाकर दिव्य अस्त्र प्राप्त किए, भीम ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, द्रौपदी ने धर्म और नीति पर गहन चर्चा की।
- उनके पास कोई स्थायी पहचान या दस्तावेज नहीं थे, फिर भी वे समाज के महत्वपूर्ण हिस्से थे।
यह वनवास का जीवन आज के घुमंतु समाज के जीवन से मिलता-जुलता है। वे भी घूमते हैं, स्थायी आवास नहीं रखते, लेकिन अपनी संस्कृति, कला और ज्ञान को जीवित रखते हैं। वनवास ने पांडवों को न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बनाया — यही वह दृष्टिकोण है जो घुमंतु समुदायों के जीवन में भी देखा जा सकता है। उनकी गतिशीलता उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी ताकत है।
(ग) जटाधारी साधु, जोगी, नट — सांस्कृतिक वाहक के रूप में

महाभारत और रामायण में घुमंतु जीवनशैली के एक अन्य महत्वपूर्ण प्रतिनिधि दिखाई देते हैं — जटाधारी साधु, जोगी, नट, गण, भिक्षुक और भटकते कवि। ये लोग तीर्थयात्रा करते थे, गाँव-गाँव घूमते थे और समाज को आध्यात्मिकता, कला और संस्कृति से जोड़ते थे।
- उनकी आजीविका थी — भिक्षा, प्रदर्शन, कथा-वाचन, आध्यात्मिक शिक्षा और लोककथाओं का प्रसार।
- वे संगीत, नृत्य, नाटक और कथा के माध्यम से समाज को जोड़ते थे।
- वे न केवल मनोरंजन प्रदान करते थे, बल्कि सामाजिक मूल्यों, धार्मिक शिक्षाओं और नैतिकता का प्रसार भी करते थे।
आज के नट, जोगी, सपेरा, बैरवा और बावरिया समुदाय इन्हीं परंपराओं के वाहक हैं। वे भी गाँव-गाँव घूमते हैं, लोकगीत गाते हैं, नृत्य करते हैं, और समाज को उसकी जड़ों से जोड़ते हैं। वे केवल कलाकार नहीं हैं, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक इतिहास के वाहक हैं।

मध्यकाल और मुगल काल: घुमंतु समाज की भूमिका — समाज, सत्ता और संस्कृति में एक अनछुआ स्तंभ
मध्यकाल और विशेष रूप से मुगल काल (1526–1857) में घुमंतु समुदायों की भूमिका केवल सांस्कृतिक नहीं, बल्कि राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इस दौरान, घुमंतु समाज को समाज के निचले स्तर पर रखे जाने के बावजूद, उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता था। उनकी गतिशील जीवनशैली, विशिष्ट कौशल और भू-ज्ञान ने उन्हें मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक और सैन्य ढांचे का एक अनिवार्य हिस्सा बना दिया।

बंजारा: मुगल सेना की जीवनरेखा
बंजारा समुदाय मुगल काल में सैन्य आपूर्ति प्रणाली की रीढ़ था। उनके बिना मुगल सेना का गतिशील अभियान असंभव था।
- अनाज का परिवहन: बंजारा टोलियाँ (गाड़ियों के काफिले) लेकर अनाज, दाल, घी, चीनी और अन्य आवश्यक सामग्री को मुगल सेना के पीछे-पीछे ले जाते थे। यह लॉजिस्टिक्स का एक ऐसा जाल था जो आधुनिक समकक्षों की तुलना में भी अत्यंत कुशल था।
- लकड़ी और ईंधन की आपूर्ति: जहाँ भी सेना जाती, बंजारा उसके लिए ईंधन, लकड़ी और तंबू सामग्री उपलब्ध कराते थे।
- सैन्य निर्माण में योगदान: मुगल किलों, महलों और ताजमहल जैसी परियोजनाओं के निर्माण में बंजारा लकड़ी और पत्थर के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे।
- सामाजिक स्थिति: बंजारा को समाज में निम्न स्तर पर रखा जाता था, लेकिन उनकी सेवाओं के कारण उन्हें सुल्तानों और सूबेदारों द्वारा सम्मान दिया जाता था। कई बार उन्हें जमींदारी या भूमि का अधिकार भी दिया गया।
नट और जोगी: दरबारों के सांस्कृतिक वाहक

नट और जोगी समुदाय मुगल दरबारों में सांस्कृतिक मनोरंजन और आध्यात्मिक संवाद के माध्यम बने।
- नट समुदाय: नट कलाकार नृत्य, अभिनय, लोकनाटक और भागवत कथा के माध्यम से लोगों को मनोरंजन देते थे। मुगल शासक अकबर जैसे उदार शासकों ने इन्हें दरबार में आमंत्रित किया। उनके नृत्य और नाटक में धार्मिक, नैतिक और सामाजिक संदेश छिपे होते थे।
- जोगी समुदाय: जोगी साधु तीर्थयात्रा करते हुए गाँव-गाँव घूमते थे। वे आध्यात्मिक शिक्षा देते थे, जाड़े के मौसम में लोगों को औषधियाँ बाँटते थे और धार्मिक कथाएँ सुनाते थे। मुगल शासकों ने कई जोगी संप्रदायों को भूमि और आश्रम दिए।
- सांस्कृतिक सेतु: ये समुदाय शहर और गाँव के बीच, हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के बीच एक सांस्कृतिक सेतु का काम करते थे। उनके गीत और कथाएँ विभिन्न भाषाओं और परंपराओं को जोड़ती थीं।
सपेरा: सांपों के विशेषज्ञ और जहर के उपचारक
सपेरा समुदाय मुगल काल में अपने विशिष्ट ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था।
- सांप पकड़ना और मनोरंजन: सपेरा लोग सांप पकड़कर गाँवों में प्रदर्शन करते थे। यह न केवल मनोरंजन था, बल्कि लोगों को सांपों से बचाव के उपाय भी सिखाया जाता था।
- जहर के उपचार में विशेषज्ञता: सपेरा समुदाय के पास सांप के जहर के उपचार का गहन ज्ञान था। वे जड़ी-बूटियों के माध्यम से जहर उतारने की प्राचीन विधियों के ज्ञाता थे। मुगल दरबारों में भी ऐसे विशेषज्ञों को रखा जाता था।
- सामाजिक भेदभाव: उनके ज्ञान के बावजूद, समाज उन्हें “अछूत” या अशुभ मानता था। उनकी कला को मनोरंजन तक सीमित रखा गया, उन्हें चिकित्सक के रूप में सम्मान नहीं मिला।

लोहार: निर्माण और सैन्य उत्पादन में योगदान
लोहार समुदाय घुमंतु नहीं था, लेकिन कई लोहार गुट अस्थायी ढांचे में काम करते थे और युद्ध के समय सेना के साथ चलते थे।
- हथियार निर्माण: लोहार मुगल सेना के लिए तलवारें, बर्चे, तोपों के पुर्जे, कवच और घोड़ों के नाल बनाते थे।
- स्थानीय कारीगरी: वे अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। कई बार उन्हें मुगल शासकों द्वारा सरकारी कारखानों में नौकरी दी जाती थी।
- गतिशीलता: कई लोहार परिवार एक स्थान पर नहीं बसते थे। वे युद्ध के मौके पर सेना के साथ घूमते थे और जहाँ भी आवश्यकता होती, वहाँ अस्थायी कार्यशाला लगा लेते थे।

घुमंतु समुदायों की सामाजिक स्थिति: सम्मान और उपेक्षा का संघर्ष
इस दौरान, घुमंतु समुदायों को दोहरी स्थिति का सामना करना पड़ा:
- सम्मान का अनुभव: उनके योगदान के कारण, मुगल शासकों ने उन्हें दरबार में आमंत्रित किया, उन्हें भूमि दी और उनकी सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया।
- उपेक्षा का सामना: फिर भी, उनकी गतिशील जीवनशैली ने उन्हें स्थायी आवास, शिक्षा और पहचान से दूर रखा। उन्हें अक्सर “अस्थिर”, “अनियंत्रित” या “असभ्य” कहा जाता था।
- पहचान का अभाव: कोई जन्म प्रमाण पत्र, आधार, राशन कार्ड नहीं था। उनकी पहचान उनके काम, कला और समुदाय के नाम पर होती थी।
प्राचीन भारत में घुमंतु जीवनशैली को कभी भी अपमानजनक या असभ्य नहीं माना गया। इसे एक वैध, सम्मानित और आवश्यक जीवन पद्धति के रूप में देखा गया। वैदिक ग्रंथों से लेकर महाकाव्यों तक, घुमंतु जीवन को न केवल स्वीकार किया गया, बल्कि उसे एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी प्राप्त था।
भगवान राम का वनवास, वानर सेना का जीवन, पांडवों का वनवास और जटाधारी साधुओं की यात्रा — ये सभी घुमंतु जीवनशैली के शास्त्रीय उदाहरण हैं, जो दिखाते हैं कि यह जीवन शैली केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक गहन सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक परंपरा है।
आज जब हम घुमंतु समुदायों को “पिछड़ा” या “असंगठित” कहते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत की संस्कृति को गाँव-गाँव तक पहुँचाया, जिन्होंने लोकगीतों के माध्यम से इतिहास सुनाया, और जिन्होंने अपनी गतिशीलता के बावजूद समाज का एक अभिन्न हिस्सा बने रहने का संकल्प लिया।
इतिहास हमें यह सिखाता है कि घुमंतु जीवनशैली कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक विकल्प के रूप में चुनी गई जीवन पद्धति है — जो प्रकृति के साथ सामंजस्य, सांस्कृतिक समृद्धि और सामाजिक लचीलेपन का प्रतीक है। उसे फिर से सम्मान देना, उसे समावेशी भारत का हिस्सा बनाना — हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

मुगल काल में घुमंतु समाज — अदृश्य आधारशिला
मुगल काल में घुमंतु समुदायों की भूमिका एक अदृश्य आधारशिला के समान थी। वे सीधे सत्ता के केंद्र में नहीं थे, लेकिन साम्राज्य के प्रत्येक पहिए को चलाने में उनका योगदान अनिवार्य था। वे सैन्य आपूर्ति के वाहक थे, सांस्कृतिक संवाद के माध्यम थे, चिकित्सा ज्ञान के धारक थे और निर्माण के कारीगर थे।
लेकिन उनकी गतिशीलता ने उन्हें स्थायी संरचनाओं — आवास, पहचान, शिक्षा, आधिकारिक दस्तावेजों — से दूर रखा। यही वह विरोधाभास था: जिनके बिना साम्राज्य नहीं चल सकता था, उन्हें फिर भी समाज के किनारे धकेल दिया गया।
यह इतिहास हमें याद दिलाता है कि घुमंतु समाज कभी “पिछड़ा” नहीं था — उसे बाद में इतना पीछे धकेल दिया गया। उनकी कला, ज्ञान और सेवाएँ भारत की सभ्यता का अटूट हिस्सा रही हैं। आज उन्हें फिर से सम्मान देना, उनकी पहचान मान्यता देना और उन्हें मुख्यधारा में लाना — न्याय की बात है।
4. ब्रिटिश शासन: घुमंतु समाज पर एक ऐतिहासिक अन्याय का युग
ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के घुमंतु समुदायों के साथ किया गया व्यवस्थित अन्याय भारतीय समाज के इतिहास में सबसे काले अध्यायों में से एक है। उनकी गतिशील जीवनशैली, जो हजारों वर्षों से भारत की संस्कृति, आर्थिक जीवन और सामाजिक ताने-बाने का अभिन्न हिस्सा रही, ब्रिटिश औपनिवेशिक दृष्टिकोण के तहत “अनियंत्रित”, “असभ्य” और “संदिग्ध” घोषित कर दी गई। इस भावना को कानूनी रूप देने के लिए 1871 में एक निर्मम कानून पारित किया गया — क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट (Criminal Tribes Act, 1871)। यह कानून न केवल निर्दोष लोगों को अपराधी घोषित करने का उपकरण बना, बल्कि घुमंतु समाज के जीवन में ऐसी गहरी चोट की जो आज तक भर नहीं पाई है।
क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, 1871: एक निर्मम कानून का जन्म
1871 में ब्रिटिश सरकार ने “क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट” को लागू किया, जिसके तहत 160 से अधिक जनजातियों और समुदायों को “जन्मजात अपराधी जातियों” (Born Criminal Tribes) की सूची में डाल दिया गया। इसमें बंजारा, नट, सपेरा, बैरवा, बावरिया, लोहार, गारसिया, टोड़ा, जोगी, बेल्ला और अनेक अन्य घुमंतु समुदाय शामिल थे।
इस कानून के तहत किए गए अन्याय:
- आवाजाही पर प्रतिबंध: घुमंतु समुदायों को एक जगह से दूसरी जगह जाने की आजादी छीन ली गई। उनकी गतिशील जीवनशैली को अपराध माना गया।
- निगरानी में रखना: उन्हें पुलिस की निगरानी में रखा गया। उनके आंदोलन को रजिस्टर में दर्ज किया जाता था।
- अपराधी के रूप में चिह्नित करना: बच्चे भी जन्म से ही “अपराधी” घोषित कर दिए गए। उनकी पहचान उनके काम या संस्कृति के बजाय एक नकारात्मक लेबल के साथ जोड़ दी गई।
- बस्तियों में बसाना: उन्हें बलपूर्वक “रिहैबिलिटेशन कैंप” या निश्चित बस्तियों में बसाया गया, जहाँ उनकी स्वतंत्रता, संस्कृति और आजीविका दोनों तबाह हो गए।

यह कानून ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति का हिस्सा था — “विभाजित करो और शासन करो”। घुमंतु समुदायों को अपराधी घोषित करके ब्रिटिश सरकार ने उनके सामाजिक बहिष्कार को बढ़ावा दिया, ताकि वे समाज के बाकी हिस्सों से अलग रहें और उनके खिलाफ पुलिस शक्ति का उपयोग आसानी से किया जा सके।
दीर्घकालिक प्रभाव: एक सामाजिक घाव
क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ने घुमंतु समुदायों के जीवन में गहरा और दीर्घकालिक नुकसान किया:
- सामाजिक भेदभाव बढ़ा: उन्हें “अपराधी जाति” के रूप में चिह्नित करने से समाज में उनके प्रति डर, घृणा और भेदभाव बढ़ गया।
- आत्मसम्मान का विनाश: पीढ़ियों तक चलने वाली उनकी संस्कृति, कला और आजीविका को अपमानित किया गया। उनके बच्चों को विद्यालयों में भी नकारा जाने लगा।
- आर्थिक विस्थापन: उनकी पारंपरिक आजीविका — यात्रा, हस्तशिल्प, मनोरंजन, पशुपालन — टूट गई।
- पहचान का संकट: उनकी पहचान अब उनकी कला या संस्कृति नहीं, बल्कि एक अपराधी लेबल थी।
1952 में रद्दाव: एक आधिकारिक समाप्ति, लेकिन वास्तविकता में जारी उपेक्षा
1952 में, स्वतंत्र भारत की सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को रद्द कर दिया और इन समुदायों को “विमुक्त जाति” (Denotified Tribes – DNT) का दर्जा दिया गया। यह एक ऐतिहासिक कदम था, लेकिन यह केवल एक कानूनी रद्दाव था — सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उपेक्षा जारी रही।
- 70 वर्ष बाद भी भेदभाव: आज भी, बंजारा, नट, सपेरा जैसे समुदायों के साथ उसी तरह का भेदभाव होता है। उन्हें गाँवों में प्रवेश नहीं मिलता, उनके बच्चों को विद्यालय में नामांकन में बाधा आती है।
- पहचान का अभाव: आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता — इन तक पहुँच अभी भी सीमित है।
- आरक्षण और योजनाओं से वंचना: इन समुदायों को SC, ST या OBC की श्रेणी में नहीं रखा गया। नतीजतन, शिक्षा, रोजगार और आवास जैसी योजनाओं से वे वंचित रहते हैं।
- पुलिस उत्पीड़न: आज भी, घुमंतु समुदायों के सदस्यों को बिना कारण गिरफ्तार किया जाता है, उन पर आरोप लगाए जाते हैं।

एक अधूरी न्याय की कहानी
क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, 1871 घुमंतु समाज के खिलाफ किए गए सबसे बड़े सामूहिक अन्यायों में से एक है। यह कानून ने न केवल उनकी आजादी छीनी, बल्कि उनकी गरिमा, पहचान और आत्मविश्वास को भी तोड़ दिया। 1952 में इसके रद्द होने के बावजूद, उसके प्रभाव आज तक जीवित हैं।
क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, 1871 घुमंतु समाज के खिलाफ किए गए सबसे बड़े सामूहिक अन्यायों में से एक है। यह कानून ने न केवल उनकी आजादी छीनी, बल्कि उनकी गरिमा, पहचान और आत्मविश्वास को भी तोड़ दिया। 1952 में इसके रद्द होने के बावजूद, उसके प्रभाव आज तक जीवित हैं।
घुमंतु समाज के साथ आज भी जो भेदभाव, उपेक्षा और अधिकारों का अभाव है, वह इसी कानून की विरासत है। इसलिए, सच्चा न्याय तभी होगा जब:
- उन्हें आरक्षण और योजनाओं में शामिल किया जाएगा।
- उनकी पहचान को मान्यता दी जाएगी।
- उनकी संस्कृति का सम्मान किया जाएगा।
- उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय के प्रति राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकारोक्ति और माफी मांगी जाएगी।
क्योंकि जब तक घुमंतु समाज को गरिमा से जीने का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक भारत का विकास अधूरा रहेगा।
6. भारत सरकार का रुख: घुमंतु समाज के उत्थान के लिए क्या कदम उठाए गए? — एक विस्तृत विश्लेषण
भारत सरकार ने घुमंतु समुदायों के उत्थान के लिए कई घोषणात्मक कदम उठाए हैं। इनमें आयोगों की स्थापना, विकास निगमों का गठन, शिक्षा नीतियों में समावेश, आवास योजनाओं का विस्तार और डिजिटल पहचान की सुविधा शामिल हैं। लेकिन इन सभी पहलों की सच्चाई यह है कि जमीनी स्तर पर इनकी प्रभावशीलता अत्यंत सीमित रही है। घुमंतु समुदायों की गतिशील जीवनशैली, पहचान के अभाव, भाषाई बाधाएँ और प्रशासनिक लापरवाही के कारण अधिकांश योजनाएँ कागजों तक सीमित रही हैं।
आइए, भारत सरकार द्वारा घुमंतु समुदायों के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों का विस्तृत विश्लेषण करें:

(1) गोविंदा नायक आयोग (1993): एक भूली हुई सिफारिश
1993 में, भारत सरकार ने गोविंदा नायक आयोग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य विमुक्त जातियों (Denotified Tribes – DNT), घुमंतु जातियों (Nomadic Tribes – NT) और अति पिछड़े वर्गों (Extremely Backward Classes – EBC) की स्थिति का अध्ययन करना और उनके उत्थान के लिए सिफारिशें देना था।
प्रमुख सिफारिशें:
- घुमंतु और विमुक्त जातियों को आरक्षण प्रदान करना।
- उनके लिए विशेष शिक्षा योजनाएँ शुरू करना।
- स्थायी आवास की व्यवस्था करना।
- रोजगार सृजन और कौशल विकास के लिए कार्यक्रम चलाना।
- उनके लिए विशेष विकास निगम की स्थापना।
वास्तविकता:
- आयोग की रिपोर्ट को अनदेखा कर दिया गया।
- आरक्षण जैसी महत्वपूर्ण सिफारिश लागू नहीं हुई।
- केंद्र और राज्य सरकारों ने इस पर कोई गंभीरता से कार्रवाई नहीं की।
- आज तक, DNT/NT समुदायों को आरक्षण नहीं मिला है, जबकि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति SC/ST से भी खराब है।
यह आयोग एक ऐसी उम्मीद थी जो घुमंतु समाज के लिए न्याय का द्वार खोल सकती थी, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में यह एक भूली हुई रिपोर्ट बनकर रह गई।

(2) राष्ट्रीय विमुक्त जाति एवं अति पिछड़ा वर्ग विकास निगम (NTDFA), 1998
1998 में, केंद्र सरकार ने NTDFA (National Denotified Tribes and Extremely Backward Classes Development Corporation) की स्थापना की। इसका उद्देश्य घुमंतु और विमुक्त जातियों के लिए ऋण, कौशल विकास, आजीविका सृजन और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक संस्थागत ढांचा बनाना था।
उम्मीदें:
- छोटे उद्यमों के लिए ऋण सुविधा।
- हस्तशिल्प, कला और पारंपरिक कौशल को बाजार से जोड़ना।
- स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
वास्तविकता:
- पहुँच अत्यंत सीमित है।
- अधिकांश घुमंतु परिवार इस निगम के अस्तित्व से अनजान हैं।
- ऋण लेने के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता, पहचान पत्र जैसी आवश्यकताएँ हैं, जो घुमंतु समुदायों के पास नहीं होतीं।
- निगम की शाखाएँ शहरों तक सीमित हैं, जबकि घुमंतु समुदाय ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहते हैं।
NTDFA एक अच्छी पहल थी, लेकिन इसका डिजाइन घुमंतु समुदायों की वास्तविक जरूरतों से दूर था। इसे एक “स्थायी निवासी” मॉडल पर आधारित बनाया गया, जबकि घुमंतु समुदाय की जीवनशैली गतिशील है।
(3) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: घुमंतु बच्चों के लिए वाचाओं की बात
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) में घुमंतु बच्चों के लिए विशेष उल्लेख किया गया है। नीति में कहा गया है कि इन बच्चों को शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए लचीले शैक्षणिक मॉडल अपनाए जाएँगे।
प्रमुख बिंदु:
- मोबाइल स्कूलों की संभावना।
- ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा का समावेश।
- स्थानीय भाषाओं में पाठ्यक्रम।
- गैर-औपचारिक शिक्षा को मान्यता।
वास्तविकता:
- कार्यान्वयन नाममात्र है।
- कोई राष्ट्रीय योजना नहीं बनाई गई।
- मोबाइल स्कूलों की अवधारणा केवल कुछ गैर-सरकारी संगठनों तक सीमित है।
- सरकारी स्कूलों में घुमंतु बच्चों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है।
- बच्चे नामांकन के बाद भी नियमित रूप से पढ़ाई नहीं कर पाते, क्योंकि उनका परिवार घूमता रहता है।
NEP 2020 ने घुमंतु बच्चों के लिए एक विचार प्रस्तुत किया, लेकिन उसे कार्यान्वित करने के लिए कोई बजट, रोडमैप या जिम्मेदार संस्था नहीं दी गई।

(4) प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): पहचान के बिना आवास असंभव
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत गरीबों को स्थायी आवास देने का लक्ष्य है। घोषणाओं में घुमंतु परिवारों को भी लाभार्थी बनाने की बात कही गई है।
वास्तविकता:
- आवास के लिए स्थायी पता और पहचान पत्र की आवश्यकता होती है।
- घुमंतु परिवारों के पास न तो आधार कार्ड है, न बैंक खाता, न जमीन का दाखिला।
- उन्हें आवास के लिए भूमि आवंटन नहीं मिलता।
- अधिकांश लाभार्थी शहरी या स्थायी ग्रामीण गरीब होते हैं, घुमंतु समुदाय वंचित रहते हैं।
कई राज्यों में घुमंतु परिवारों को आवास योजना से बाहर रखा गया है। जहाँ कहीं आवास दिया गया, वहाँ भी वे उसे छोड़कर फिर से यात्रा पर निकल जाते हैं, क्योंकि उनकी आजीविका घूमने पर निर्भर है।
(5) आधार कार्ड और डिजिटल पहचान: एक अधूरी क्रांति
आधार कार्ड और डिजिटल भारत के तहत पहचान की सुविधा बढ़ी है। आधार कार्ड के बिना कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता।
चुनौतियाँ:
- नेटवर्क की कमी: दूरदराज के इलाकों में नेटवर्क नहीं होता, जिससे आधार बनाना मुश्किल होता है।
- भाषाई बाधा: आधार रजिस्ट्रेशन अंग्रेजी या हिंदी में होता है, जबकि घुमंतु समुदाय स्थानीय भाषाएँ बोलते हैं।
- जागरूकता की कमी: कई परिवारों को नहीं पता कि आधार क्या है या इसके लिए कहाँ जाना है।
- दस्तावेजों का अभाव: आधार बनाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र या पते का प्रमाण चाहिए, जो घुमंतु परिवारों के पास नहीं होता।
कुछ संगठनों ने मोबाइल आधार शिविर लगाकर इस समस्या को कम किया है, लेकिन यह अभी भी सीमित पैमाने पर है।
(6) आयुष्मान भारत: स्वास्थ्य बीमा, लेकिन लाभ कहाँ?
आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा गरीब परिवारों को दिया जाता है। घुमंतु परिवारों को भी इसका लाभ देने की बात कही गई है।
वास्तविकता:
- आयुष्मान कार्ड के लिए आधार कार्ड और बैंक खाता आवश्यक है।
- घुमंतु परिवारों के पास ये नहीं होते।
- उनके पास स्थायी पता नहीं होता, जिसके कारण रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता।
- जब वे अस्पताल जाते हैं, तो उनसे दस्तावेज मांगे जाते हैं, जिसके कारण उपचार में देरी होती है।
परिणामस्वरूप, घुमंतु परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच नहीं मिल पाती। टीकाकरण, मातृ स्वास्थ्य, बाल रोग जैसी सुविधाएँ उनसे वंचित रहती हैं।

एक अधूरा वादा
भारत सरकार ने घुमंतु समुदायों के उत्थान के लिए कई घोषणाएँ की हैं, लेकिन कार्यान्वयन और जमीनी वास्तविकता के बीच एक विशाल खाई है। अधिकांश योजनाएँ स्थायी निवासी मॉडल पर आधारित हैं, जबकि घुमंतु समुदाय की जीवनशैली गतिशील है।
सरकार को इन समुदायों के लिए विशेष, लचीले और गतिशील मॉडल विकसित करने होंगे। आवश्यकता है:
- घुमंतु समुदायों के लिए एक राष्ट्रीय नीति।
- उन्हें आरक्षण देना।
- मोबाइल शिक्षा, स्वास्थ्य और पहचान सेवाएँ शुरू करना।
- स्थायी आवास के विकल्प बनाना, जो उनकी आजीविका के साथ सामंजस्य रखते हों।
जब तक सरकार घुमंतु समुदायों को “समस्या” नहीं, बल्कि “संस्कृतिक धरोहर” मानेगी, तब तक कोई योजना सफल नहीं होगी। उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय के प्रति स्वीकारोक्ति और न्याय की बात तभी होगी जब उन्हें गरिमा, पहचान और अधिकार मिलेंगे।
एक समावेशी भारत के लिए आह्वान — घुमंतु समाज का उत्थान, राष्ट्र की नैतिक जिम्मेदारी
घुमंतु समाज केवल एक समुदाय नहीं है — वे भारत की सांस्कृतिक आत्मा का एक जीवंत हिस्सा हैं। उनके लोकगीत, नृत्य, कला, हस्तशिल्प, पारंपरिक ज्ञान और जीवनशैली भारत की विविधता का अमूल्य खजाना हैं। वे वह धारा हैं जो हजारों वर्षों से भारत की सड़कों, गाँवों, जंगलों और तीर्थस्थलों पर घूमते हुए इस सभ्यता को जीवंत रखे हुए हैं। उनके गीत में मिट्टी की गहराई है, उनके नृत्य में प्रकृति का ताल है, उनके हाथों में सदियों का कौशल है। लेकिन आज, जब भारत डिजिटल भारत, स्मार्ट सिटीज और विकसित राष्ट्र की बात कर रहा है, तब भी ये लोग आधुनिक भारत के मुख्यधारा से दूर हैं।
यह सिर्फ एक सामाजिक विसंगति नहीं, बल्कि एक नैतिक संकट है। घुमंतु समाज के साथ हो रहा भेदभाव, उपेक्षा और अधिकारों से वंचना भारत के संवैधानिक मूल्यों — समानता, न्याय और सम्मान — के खिलाफ है। जब तक हर भारतीय को गरिमा से जीने का अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक हमारा विकास अधूरा है। घुमंतु समाज के उत्थान के बिना, भारत का सच्चा विकास असंभव है।

भारत सरकार के कदम: इरादे अच्छे, प्रभाव सीमित
भारत सरकार ने घुमंतु समुदायों के उत्थान के लिए कई घोषणाएँ की हैं — गोविंदा नायक आयोग, NTDFA, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, आधार कार्ड, आयुष्मान भारत, PMAY। लेकिन इनकी प्रभावशीलता जमीनी स्तर पर अत्यंत सीमित रही है। यह इसलिए है क्योंकि अधिकांश योजनाएँ स्थायी निवासी मॉडल पर आधारित हैं, जबकि घुमंतु समाज की जीवनशैली गतिशील है। उनके लिए आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और पहचान के लिए अलग, लचीले और गतिशील समाधानों की आवश्यकता है।
एक समावेशी भारत के लिए आह्वान
घुमंतु समाज के उत्थान के लिए अब सिर्फ योजनाओं की नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय संकल्प की आवश्यकता है। यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की नैतिक जिम्मेदारी है। इस दिशा में निम्नलिखित कदम तुरंत उठाए जाने चाहिए:
1. एक राष्ट्रीय नीति घुमंतु समाज के लिए
भारत को घुमंतु समाज के लिए एक विशेष राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता है, जो उनकी गतिशील जीवनशैली को समझे और उसके अनुकूल समाधान प्रस्तावित करे। यह नीति शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, आजीविका, पहचान और सामाजिक सम्मान सभी पहलुओं को कवर करे।
2. डिजिटल पहचान और शिक्षा के लिए विशेष योजनाएँ
- मोबाइल आधार शिविर को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया जाए।
- ऑफलाइन शिक्षा ऐप्स स्थानीय भाषाओं में विकसित किए जाएँ।
- सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल वैन के जाल को बढ़ाया जाए।
- घुमंतु बच्चों के लिए लचीले नामांकन नियम बनाए जाएँ।
3. स्थायी आवास और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बजट आवंटन
- घुमंतु परिवारों के लिए स्थायी आवास के विकल्प बनाए जाएँ, जो उनकी आजीविका के साथ सामंजस्य रखते हों।
- घुमंतु विकास कोष स्थापित किया जाए, जो ऋण, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा दे।
- उनकी पारंपरिक कला और हस्तशिल्प को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए।
4. सामाजिक भेदभाव के खिलाफ जागरूकता अभियान
- स्कूली पाठ्यक्रम में घुमंतु समाज के योगदान को शामिल किया जाए।
- मीडिया और सिनेमा के माध्यम से उनकी संस्कृति को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाए।
- सामाजिक भेदभाव, पुलिस उत्पीड़न और अपमान के खिलाफ राष्ट्रीय जागरूकता अभियान चलाए जाएँ।
घुमंतु समाज के बिना, भारत अधूरा है

घुमंतु समाज को सिर्फ गरीबी उन्मूलन का विषय नहीं माना जाना चाहिए। यह एक सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक मुद्दा है। उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय — विशेष रूप से क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, 1871 — के प्रति राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकारोक्ति और माफी मांगी जानी चाहिए।
उन्हें आरक्षण, शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच देना न्याय की बात है। उनकी कला, ज्ञान और संस्कृति को सम्मान देना राष्ट्र की जिम्मेदारी है।
भारत की वास्तविक शक्ति उसकी विविधता में है। जब तक हम घुमंतु समाज को गरिमा, पहचान और अधिकार नहीं देंगे, तब तक हमारा विकास केवल आँकड़ों तक सीमित रहेगा। एक सच्चा विकसित भारत वह होगा, जहाँ हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार मिले, हर महिला को गरिमा से जीने का अधिकार मिले, और हर नागरिक को अपनी पहचान के साथ जीने का अधिकार मिले।
घुमंतु समाज के उत्थान के बिना, भारत का सच्चा विकास असंभव है। यह समय है कि हम इस विसंगति को स्वीकार करें और एक समावेशी, न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण भारत के लिए काम करें।