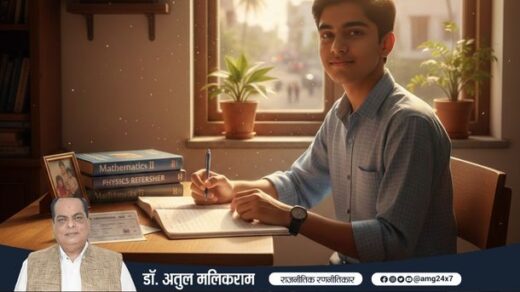आज जब रसोई में स्टील के डब्बों से लेकर माइक्रोवेव की बीप तक सब कुछ शोर करता है, तब अनायास ही स्मृति में गूँज उठती है वह धीमी-धीमी आवाज़ चूल्हे के नीचे जलती लकड़ी की चिट-चिट की.. और वह कभी न भूली जा सकने वाली याद.. आँच पर सौंधी-सी रोटी पकने की, पीतल की कढ़ाही में सरसों के तेल की आती खुशबू की और उसके साथ कानों में सुनाई पड़ती दादी माँ की मीठी-सी गुनगुनाहट की।
सच-मुच दादी की रसोई कोई साधारण रसोई नहीं थी, वह तो एक जीवंत किताब थी, जिसमें स्वाद, स्वास्थ्य, परंपरा और संवेदना, सब कुछ साथ-साथ पका करता था। मिट्टी के चूल्हे पर रोटियाँ फूलतीं, और ताजे घी की महक पूरे घर को अपने आगोश में भर लेती। और फिर, जब दादी एक किनारे बैठकर सबसे पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालतीं, तब लगता, जैसे रसोई नहीं, एक धर्म का घर हो।
लेकिन, अब तो वह रसोई, सारे संस्कार, सादगी और स्नेह के साथ, एक अनसुने सन्नाटे के साथ हमारे जीवन से पलायन कर चुकी है। हर दिन का भोजन अब महज़ भूख मिटाने का माध्यम बन गया है। दादी माँ की रसोई में जो भाव था, जो मौसमी समझ और आयुर्वेदिक संतुलन हुआ करता था, वह सब अब रेफ्रिजरेटर की प्लास्टिक ट्रे में सिमटकर रह गया है। गर्मियों के मौसम में मशहूर वह कैरी का पना अब बॉटल में आता है, सर्दियों में घर पर बनने वाले सूखे मेवे, मैथी दाने और उड़द के लड्डू भी तो अब मिठाई की दुकान से खरीदे जाते हैं, और तो और बरसात की वो गरमा-गर्म पकौड़ियाँ और चाय भी अब किसी कैफे के मेन्यू कार्ड पर पड़ी होती हैं। यह बात और है कि स्वाद से उसका कोई लेना-देना नहीं..
दादी माँ बिना किसी डिग्री के एक चलती-फिरती औषधशाला थीं। उनके “थोड़ी-सी अजवायन भी डाल दो” में पेट के हर दर्द की दवा हुआ करती थी, और “इसमें गुड़ डालो, गला ठीक रहेगा” में मौसम के बदलते मिज़ाज की समझ। यह कोई रट कर सीखी हुई विद्या नहीं थी, यह अनुभव की सौंधी-सौंधी परतों से निकला जीवन-सिद्ध ज्ञान था। दादी कहा करती थीं, “बेटा, जो खाना दवा बन जाए, वही असली खाना होता है।” और सच मानिए, उस समय का हर निवाला शुद्ध था, स्वास्थ्यवर्धक था, और सबसे बड़ी बात वह संजीवनी जैसा था। आज वह खाना महज़ कैलोरी बन कर रह गया है.. और दादी, एक धुँधली-सी परछाईं।
अब की रसोई सिर्फ स्टेनलेस स्टील की अलमारियों और स्मार्ट डिवाइसेज़ का कोना बन चुकी है। जहाँ कभी हँसी-ठिठोली में पकते थे पराठे, अब वहाँ साइलेंट चिमनी की भूले-चूके आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। सब कुछ ‘क्विक’ और ‘इंस्टेंट’ हो गया है। फूड डिलीवरी ऐप्स के नोटिफिकेशन अब दादी की पुकार को निगल चुके हैं। गरम रोटी के साथ पिघलता मक्खन अब सिर्फ गूगल में सर्च किए हुए फोटोज़ में ही तो रह गया है, और असल ज़िंदगी में तो अब डिब्बाबंद स्वाद का राज चलता है।
दादी की रसोई दरअसल एक पाठशाला थी, जहाँ हर काम अपने आप में एक संस्कार था। आटे को गूँथते समय धैर्य सिखाया जाता था, सब्जी काटते हुए एकाग्रता का पाठ पढ़ाया जाता था और मसालों को तवे पर भूनते समय सही समय पर प्रतिक्रिया देना सिखाया जाता था। यह सब कुछ बिना किसी प्रवचन के, रोज़मर्रा के जीवन में घुला हुआ पाठ था। लेकिन, आज के बच्चों के हाथ में बेलन नहीं, मोबाइल है, रोटी की गोलाई अब उतनी मायने नहीं रखती, जितना मायने रखता है वीडियो कॉल का सही एंगल।
उनकी रसोई में सिर्फ स्वाद नहीं, सह-अस्तित्व का भाव पकता था। हर जीव के लिए एक हिस्सा रखा जाता था.. गाय के लिए पहली रोटी, कुत्ते के लिए आखिरी, चींटियों के लिए आटा। पुराने समय में रसोई सिर्फ इंसानों के लिए नहीं थी, पूरी सृष्टि के लिए अर्पण हुआ करती थी। उस रसोई का तो पलायन हो चुका है.. अब वहाँ मॉड्यूलर किचन रहने लगा है, जहाँ बेआवाज़ भूख के लिए कोई दराज नहीं बनी.. वहाँ सिर्फ चमकदार बर्तनों की सजावट है, जिसमें करुणा का कोई कोना नहीं।
आज का मॉडर्न ज़माना इतना खोखला है कि उनके असल जीवन में दादी की रसोई का भले ही कोई महत्व न हो, लेकिन हैश टैग लगाकर ‘दादी की रसोई’ खूब ट्रेंड करेगा.. और तो और ऐसे ही किसी जज़्बाती नाम से खुले रेस्तरां से खाना मँगाकर खाना भी उन्हें खूब लुभाएगा।
बताओ क्यों.. क्योंकि असल में दादी के हाथ की फुल्के वाली गोल-गोल रोटियों को बनने में समय लगता है, और यहाँ तो सब कुछ ‘इन मिनट्स डिलीवर’ चाहिए, फिर भले ही कितनी देर पहले की बनी हुई रोटियाँ उस डिलीवरी के साथ आ रही हों.. उससे क्या ही फर्क पड़ता है। दादी की रसोई को तो हमने ऐड शूट्स में कैद करके रख दिया है, जहाँ हाथ नहीं, स्क्रिप्ट चलती है। अब कहानियाँ बुनती नहीं रोटियाँ, अब बटर चिकन की प्लेट के साथ नोस्टैल्जिया फ्री मिलता है।
दीवार पर टंगी उनकी पुरानी तस्वीर भी शायद यही सोचकर मुस्कुराती है कि क्या कोई फिर से उस मिट्टी की सौंधी खुशबू को वापस लाएगा? क्या कोई फिर से चूल्हे की आँच में अपनी थकान मिटाएगा?
रसोई का यह पलायन महज़ कुछ व्यंजनों का नहीं, बल्कि हमारी पूरी जीवनशैली का है। यह उन संबंधों का विस्थापन है, जो पकते-पकते और भी गहरा रंग लाते थे। जो रोटियाँ सिर्फ पेट नहीं भरती थीं, बल्कि रिश्तों को भी सींचती थीं। आज आधुनिकता ने हमें खूब सुख-सुविधा दी है, लेकिन वह आत्मीयता नहीं दे सकी, जो दादी माँ अपने हाथों की छुअन से रोटियों में भर देती थीं।
यदि हम चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी भी खाने को सिर्फ पेट भरने का नहीं, आत्मा को तृप्त करने का माध्यम समझे, तो हमें फिर से उन स्मृतियों की रसोई की ओर लौटना होगा। हमें गैस पर तवे की जगह मिट्टी की महक महसूस करनी होगी, और रेसिपी से ज्यादा रिश्तों पर ध्यान देना होगा।
हमें इस सच को सच मानना होगा कि रसोई सिर्फ ईंधन और भोजन का स्थान नहीं होती, वह प्रेम, परंपरा और परवरिश की पहली पाठशाला होती है। वहाँ हर कड़ाही में संस्कार पकते थे, हर मसाले में स्मृति पिसती थी और हर रोटी में स्नेह पलता था। और दादी माँ.. वे उस अनमोल परंपरा की पहली कवयित्री थीं, जिनके छंद आज भी हमारी स्मृति में महकते हैं। तो अभी-भी देर नहीं हुई है, रसोई अभी ज्यादा दूर नहीं गई है.. इसे पहले कि वह हमसे इतनी दूर चली जाए कि फिर कभी वापस न आ सके, उसके पलायन को रोक लीजिए..